पढ़िये सुदर्शन की कहानी “कवि की स्त्री” (Kavi Ki Stree Story By Sudarshan In Hindi) – सुदर्शन की यह रचना पति पत्नी के प्रेम की कहानी है, जहाँ निशब्द एवं निर्मल प्रेम का वर्णन किया गया है. Kavi Ki Stree Sudarshan Ki Kahani में :
Kavi Ki Stree Story By Sudarshan In Hindi
Table of Contents
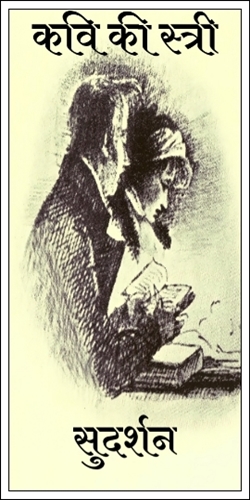
(1)
सत्यवान
छात्रावस्था में मैं और मणिराम साथ-ही-साथ पढ़ते थे। उस समय हम एक-दूसरे पर प्राण देते थे। वे बचपन के दिन थे। जब तक एक-दूसरे को देख न लेते, शांति न मिलती। उस समय हमें बुद्धि न थी। पीछे से प्रेम का स्थान बैर ने ले लिया था, दोनों एक-दूसरे के लहू के प्यासे हो गए थे। तब हम शिक्षित हो चुके थे। एफ.ए. की परीक्षा पास करने के पश्चात् हमारे रास्ते अलग-अलग हो गये। मणिराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गये। मैंने साहित्य संसार में पाँव रखा। मुझे रूपये-पैसे की परवाह न थी। पूर्वजों की संपत्ति ने इस ओर से निश्चिंत कर दिया था। दिन-रात कविता के रस में तल्लीन रहता। कई-कई दिन घर से बाहर न निकलता। उन दिनों मेरे सिर पर यही धुन सवार रहती थी। एक-एक पद पर घंटों खर्च हो जाते थे। अपनी रचना को देखकर मैं गर्व से झूमने लग जाता था। कभी-कभी मुझे अपनी कविता में तुलसीदास की उपमा और सूरदास के रूपकों का स्वाद आता था। जब मेरी कवितायें पत्रों में निकलने लगीं, तब मेरा कवित्व का मद उतरने लगा। मद उतर गया, पर उसका नशा न गया। वह नशा प्रख्याति, कीर्ति और यश का नशा था। थोड़े ही वर्षों में मेरा नाम हिंदी संसार में प्रसिद्ध हो गया। मैं अब कुछ काम न करता था। केवल बड़े-बड़े लोगों को पार्टियाँ दिया करता था। अब इसके बिना मुझे चैन न मिलता था। कविता में इतना मन न लगता था। पहले मेरा सारा समय इसी की भेंट होता था, पर अब वह जी-बहलावे की चीज़ हो गयी थी। परन्तु जब कभी कुछ लिखता, रंग बांध देता था। तुच्छ से तुच्छ विषय को लेता, तो उसमें भी जान डाल देता था।
उधर मणिराम चिकित्सा के ग्रंथों के साथ सिर फोड़ता रहा। पांच वर्ष बाद असिस्टेंट सर्जरी की परीक्षा पास करके उसने अपनी दुकान खोल ली। परीक्षा का परिणाम निकलने के समय उसका नाम एक बार समाचार-पत्र में निकला था। इसके पश्चात् फिर कभी उसका नाम पत्रों में नहीं छपा। इधर मेरी प्रशंसा में प्रति दिन समाचार-पत्रों के पृष्ठ भरे रहते। वह दुकान पर सारा दिन बैठा रोगियों की बाट देखता रहता था। परन्तु उसका नाम कौन जानता था? लोग जाते हुए झिझकते थे। मैं उसकी ओर देखता तो घृणा से मुँह फेर लेता, जिस प्रकार मोटर में चढ़ा हुआ मनुष्य पैदल जानेवालों को घृणा से देखता है।
(2)
एक दिन एक पत्र आया। उसमें मेरी कवित्व कला की बहुत ही प्रशंसा की गयी थी। मेरा अस्तित्व देश और जाति के लिए सम्मान और गौरव का हेतु बताया गया था। मेरे पास ऐसे पत्र प्रायः आया करते थे। यह कोई नई बात न थी। कभी-कभी तो ऐसे पत्रों को देखकर झुंझला उठता था। हम पुरुषों की ओर से उपेक्षा कर सकते हैं, परन्तु किसी कोमलांगी के साथ यह व्यवहार करने को जी नहीं चाहता और यह भी किसी साधारण स्त्री की और से न था। इसकी लेखिका देहरादून के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हृदयनारायण की शिक्षिता लड़की सावित्री थी, जिसने इसी वर्ष बी.ए. की परीक्षा पास की थी। जिसके संबंध में समाचार-पत्रों में कई लेख निकले थे, परन्तु मैंने उन्हें पढ़ने की आवश्यकता न समझी थी। इस पत्र ने सब कुछ याद करा दिया। मैंने उसी समय लेखनी पकड़ी, और जवाब लिखने बैठ गया। परन्तु हाथ जवाब दे रहे थे। ऐसी लगन से कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा के पर्चे भी न लिखता होगा। एक-एक शब्द पर रुकता था, और नये-नये शब्द ढूंढकर नये-नये विचार लेखनी के अर्पण करता जाता था। मैंने सावित्री और उसकी विद्वता की प्रशंसा में कोष के संपूर्ण सुंदर शब्द समाप्त कर दिये। अपनी तुच्छता को भी अंगीकार किया—“आप मेरी प्रशंसा करती हैं, यह आपका बड़प्पन है, अन्यथा मेरी कविता में धरा ही क्या है? न कल्पना में सौंदर्य है, न शब्दों में मिठास। रसिकता कविता का प्रधान अंग है, वह मेरी कविता से कोसों दूर है। हम कवि बन बैठते हैं, परन्तु कवि बनना आसान नहीं। इसके लिए देखने वाली आँखें और सुनने वाले कान दोनों की आवश्यकता है,”—इत्यादि। कहने की आवश्यकता न होगी कि अपनी प्रशंसा करने का यह एक सभ्य ढंग है।
कुछ दिन पश्चात् इस पत्र का उत्तर आया—“यह जो कुछ आपने लिखा है, आप-जैसे महापुरुषों के योग्य ही है, अन्यथा मैं तो आपको टेनिसन और वर्ड्सवर्थ से बढ़कर समझती हूँ। आप कहते हैं कि आपकी कविता रस-हीन है, होगी! परन्तु, मुझ पर तो यह जादू का काम करती है। घंटों रस-सागर में डुबकियाँ लगाती हूँ। खाना-पीना भूल जाती हूँ। जी चाहता है, आपकी लेखनी चूम लूं।“
यह पत्र शराब की दूसरी बोतल थी। अंतिम वाक्य ने हृदय में आग लगा दी। मैंने फिर उत्तर दिया, पत्र में हृदय खोलकर रख दिया। कवि अपने चाहने वालों को आकाश में चढ़ा देते हैं। मैंने सावित्री की प्रशंसा में आकाश-पाताल एक कर दिया। लिखा—‘लाइल का कथन है कि कवि केवल वही नहीं, जो कविता कर सकता है, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति जो कविता समझ सकता है, और उसके मर्म तक पहुँच सकता है, कवि है। इस रूप में तुम भी कवि हो। मैंने अच्छे-अच्छों को देखा है, कविता के महत्व को नहीं समझ सकते। परन्तु तुम तो बाल की खाल निकालती हो। तुम्हारी योग्यता पर मुझे आश्चर्य होता है। धन्य है भारत भूमि, जिसमें तुम-जैसी देवियाँ खेलती हैं। ’
मैंने सैकड़ों उपन्यास पढ़े थे, अच्छी-से-अच्छी कवितायेँ देखी थीं, परन्तु जो रस, जो स्वाद सावित्री के पत्र में था, वह किसी में न पाया। यही जी चाहता था कि उन्हीं को पढ़ता रहूं।
(3)
सावित्री
निस्संदेह वे मुझे चाहते हैं, अन्यथा इस प्रकार तुरंत ही उत्तर-प्रत्युत्तर न देते। आज पत्र लिखती हूँ, तीसरे दिन उत्तर आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो मेरे पत्र की राह देख रहे थे। उनके पत्र उनके कवित्व से अधिक सरस हैं। पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है। और कभी-कभी तो ऐसी चुटकी लेते हैं कि मन अधीर हो उठता है। मैंने चित्र मांग भेजा था। उत्तर देते हैं—“तुमने लिखा है कि चित्र भेज रही हूँ, परन्तु मुझे आज तक नहीं मिला। रजिस्ट्री की रसीद तो भेज दो, डाकखाने पर नालिश कर दूं।“ बरबस मुझे अपना चित्र भेजना पड़ा, उत्तर में उनका चित्र आ गया। मेरा विचार सच्चा निकला। कैसे रसीले हैं! मुख पर राजकुमारों जैसा लावण्य झलकता है। मेरे हृदय को पहले ही चैन न था, चित्र ने रहा-सहा भी छीन लिया। रात को नींद नहीं आती। उनकी अंतिम कविता ने उनका हृदय मुझ पर खोल दिया है। ‘प्रियतमा से’- कैसा प्यारा शीर्षक है! अक्षर-अक्षर से प्रेम टपकता है। इससे पहिली कविता ‘पाती निहारकर’ भी मुझ पर ही लिखी गई थी। लिखती हूँ, तुम मुझे कलंकित करके छोड़ोगे। यह तो कहो, तुम मेरे पीछे पल्ले झाड़कर क्यों पड़ गए हो? एक और कविता ‘एकांत में’ प्रकाशित हुई है। इससे जान पड़ता है, अभी तक कुँवारे हैं। तो मेरी….परन्तु वे इतना परिश्रम क्यों करते हैं? बहुत पढ़ना-लिखना मनुष्य को बांस की तरह खोखला कर देता है। लिखती हूँ, कविता करना बंद कर दो और अपने शरीर की ओर ध्यान दो। मुझे बड़ी चिंता रहती है। इसके बाद मैंने उनके संबंध में सब-कुछ मालूम कर लिया। वे हमारी बिरादरी के हैं, और कुँवारे हैं।
मैंने पत्र लिखा। पहले पत्रों और इस पत्र में बहुत भेद था। इसमें कोई ‘संकोच’, कोई ‘बनावट’ न थी—“तुम्हारे पत्रों से संतोष नहीं होता। जी चाहता है, प्रत्यक्ष दर्शन हों, तो गिरकर आप के पैरों को चूम लूं। अब अधिक न तरसाओ। प्रतिक्षण सामने देखना चाहती हूँ। प्रायः सोते-सोते चौंक पड़ती हूँ। सोचती हूँ, तुम्हारे खाने-पीने का क्या प्रबंध होता होगा। रात को अधिक समय तक जागते तो नहीं रहते? स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा, इसका पूरा ध्यान रखो। मुझे पत्र लिखना न भूलो। जी डर जाता है। मुझे अपने चरणों की दासी समझो।”
चौथे दिन उत्तर आया, तब मैं जमीन से उछल पड़ी। वे मेरे साथ विवाह करने के लिए सहमत नहीं, प्रत्युत अधीर हो रहे थे। मैंने आँखें बंद कर लीं, और आनेवाले काल्पनिक सहवास का चिंतन करके आनंद के झूले में झूलने लगी। इतने में किसी के पैरों की चाप सुनाई दी, मेरी आँखें खुल गई। देखा, छोटा भाई प्रभाशंकर चित्रों का एक बण्डल हाथ में लिए खड़ा है। मैंने आश्चर्य से पूछा, “प्रभा, यह क्या है?”
“बाबूजी कहते हैं, ये चित्र देखकर एक छांट दो। प्रत्येक चित्र के साथ-साथ एक पत्र है, उसे भी पढ़ जाना।”
यह कहते-कहते प्रभा ने वह बण्डल मेरे हाथ में दे दिया, और तेजी से बाहर निकल गया।
मैंने बण्डल खोला। इसमें उन पुरुषों के फोटो थे, जो मेरे साथ विवाह करना चाहते थे। मैंने मुस्कराते हुए सब पर एक उचटती हुई दृष्टि डाली। कोई बैरिस्टर था, कोई इंजीनियर, कोई ठेकेदार, परन्तु मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। मेरे अंतःकरण में एक ही मूर्ति के लिए स्थान था, और वहाँ पहले ही से वह मूर्ति विराजमान थी। फुर्ती से उठकर मैंने अपना संदूक खोला, और उसमें से उनका फोटो निकालकर उसपर Passed शब्द लिखकर उसे बाबूजी के पास भेज दिया। वे स्तंभित रह गये। उन्हें यह आशा न थी। वे समझते थे, मैं कोई लखपति का बेटा पसंद करूंगी, परन्तु मैंने एक कवि को चुना। वे निर्धन न थे, पर इतने धनाढ्य भी न थे। मेरे चाहने वालों में कई पुरुष ऐसे थे, जो उनको खरीद सकने का सामर्थ्य रखते थे। परन्तु प्रेम अंधा कहा गया है, उसे देखना किसने सिखाया है? बाबूजी मेरी इच्छा के अनुसार सहमत हो गये। उन्होंने मुझे लाड़-प्यार से पाला था। मेरी शिक्षा पर सहस्त्रों रूपये खर्च किये थे। इस विषय में भी उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी।
(4)
जिस बात का भय था, अंत में वही हुआ। उन्हें बुखार आने लगा है। कुछ दिन हुए, उनके एक मित्र मिलने आये थे। वे कहते हैं कि डॉक्टरों को तपेदिक का संदेह है। यह बात सुनकर बाबूजी बड़े व्याकुल हुये। सदैव उदास रहते हैं, जैसे कोई रोग लग गया हो। उनकी इच्छा है कि मैं अब इस विवाह का विचार छोड़ दूं। जलती आग में कूदना बुद्धिमता नहीं है। परन्तु, मैं इसकी परवाह नहीं करती। संसार की आँखों में हम कुँवारे हैं, पर जब मन मिल गए, प्रेम की डोर बंध गयी, तब शेष क्या रह गया? अब मैं उनकी हूँ, और कोई रोग, कोई शक्ति, कोई बला मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मृत्यु को भी यह साहस नहीं। सावित्री ने सत्यवान को यमदूत के पंजे से छुड़ा लिया था। क्या मैं इन्हें नहीं बचा सकूंगी? मैं भी सावित्री हूँ। इसी भारत की मिट्टी से मेरा जन्म हुआ है, मैं उसके कारनामे को फिर ज़िन्दा कर दिखाऊंगी।
सायंकाल हो गया था, बाबूजी अपने कमरे में बैठे थे। मुझे चिंता हुई। यह समय उनके क्लब जाने का था। सर्दी-गर्मी में बराबर जाते थे। यह उनका नियम था- जिसमें कभी त्रुटि न आती थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई, और धीरे-से बोली-“क्यों, आज आप क्लब नहीं गये?”
बाबूजी ने कोई उत्तर न दिया।
मैंने कहा-“आप उदास दिखाई देते हैं?”
बाबूजी ने कहा-“तुम्हें इससे क्या?”
“आपका स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा।”
“कोई परवाह नहीं।”
“आपका खाना आधा भी न रहा।”
“मैं यह सब कुछ जानता हूँ।”
“किसी डॉक्टर को दिखाइये, रोग का बढ़ाना अच्छा नहीं।”
“अब मेरा डॉक्टर यमराज ही होगा!”
मेरी आँखों में आँसू आ गये, सिर नीचे झुक गया। बाबूजी दूसरी ओर देख रहे थे, परन्तु मेरे आँसू उन्होंने देख लिये। बातचीत का रंग बदल गया। वे बोले-“सावित्री, मैं तो अपने भाग्य को रो रहा हूँ, परन्तु तुम्हें क्या हुआ है?”
मैंने उनकी और इस प्रकार देखा, जैसे उन्होंने मुझ पर कोई बड़ा अत्याचार किया हो, और कहा—“आप मेरे पिता हैं, क्या आप भी मेरे इन आँसुओं का रहस्य नहीं समझते? आपकी प्रत्येक बात छिपी कटार है, प्रत्येक वचन विष में बुझा हुआ बाण। आपके मित्र हैं, सुहृद हैं, काम-काज हैं, क्लब है। आप बाहर चले जाते हैं, मैं बैठी कर्मों को रोती हूँ। मैं लड़की हूँ। लड़कियों के मुँह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। परन्तु क्या करूं? देखती हूँ, मेरे जीवन का सर्वस्व लुट रहा है। चुप कैसे रहूं? आप देर करके मेरे भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं।”
बाबूजी ने आतुर होकर कहा-“परन्तु सावित्री, देखकर मक्खी निगलना आसान नहीं। क्या तुझे विश्वास है, कि वह तेरी सेवा-सुश्रुषा से अच्छा हो जायेगा?”
“हाँ, मुझे विश्वास है, कि मैं उन्हें बचा लूंगी। कवि बे-परवाह होते हैं, प्रायः पढ़ने-लिखने में लगे रहते हैं। मैं उन्हें जीवन के समस्त झंझटों से निश्चिंत कर दूंगी। कहूंगी—पहले अपने स्वास्थ्य की और देखो, पीछे कविता भी हो लेगी। नौकरों के हाथ की रोटियाँ खाते हैं, खाया-पिया क्या तन लगेगा? स्तुति करने को सभी हैं, सहानुभूति किसी में नाम की नहीं।”
बाबूजी पर मेरी इन बातों का बहुत ही प्रभाव हुआ। कुछ समय के लिए उनका मुँह बंद हो गया। फिर बोले—“यह सब ठीक है, परन्तु कहने और करने में बहुत भेद है। मुझे संदेह है, कि जो कुछ तुम कह रही हो, उसे कर भी सकती हो, या नहीं।”
मेरा मुख लाल हो गया—जैसे भरे-बाजार में सिर से दुपट्टा उतर गया हो। फिर संभलकर बोली—“मैं अपने वचनों के उत्तरदायित्व से अपरिचित नहीं। जो-कुछ कहा है, करके दिखा दूंगी।”
“यह सब भावना की बातें हैं, समय पर धुयें की नाईं उड़ जाती हैं।”
“मेरे विचार में संसार भावनाओं पर ही जीता है।”
बाबूजी चुप हो गये, कोई उत्तर न सूझा। थोड़ी देर सिर झुकाकर सोचते रहे। तब एकाएक उठे, और मुझसे कुछ कहे-सुने बिना बाहर चले गये।
(5)
विवाह हो गया। वह बात झूठी निकली। उन्हें कोई रोग न था। यह सब किसी की क्षुद्रता थी। उनका स्वास्थ्य देखकर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। मुख पर लाली है, नेत्रों में ज्योति। मुझे देखते ही कली की नाईं खिल जाते हैं। मैंने कई कवियों के चरित्र पढ़े हैं, और एक दोष प्रायः सब में पाया है। वह यह, कि उनका आचरण कुछ इतना पवित्र नहीं होता। परन्तु उनके विषय में यह कल्पना करना भी पाप है।
वह बहुत ही शर्मीले हैं; किसी पराई स्त्री के सामने आँख नहीं उठाते। वह इसे भी सदाचार से गिरा हुआ समझते हैं। मेरी कोई सहेली आ जाती, तो उठकर अंदर चले जाते थे। मैं बहुतेरा समझाती हूँ। कहती हूँ, तुम मर्द हो, यदि स्त्री पर्दा नहीं करती, तो पुरुष क्यों करे? परन्तु वह हँसकर टाल देते हैं। मुझे उन पर पूरा-पूरा विश्वास है। मैं समझती हूँ, सब कुछ हो सकता है, परन्तु उनके मन में मैल नहीं आ सकता। ऐसा पुरुष मिल जाना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने अपने-आपको मुझ पर छोड़ दिया है। घर-बाहर का स्याह सफ़ेद सब मेरे ही हाथ में है। कपड़े तक स्वयं नहीं बदलते। यदि मैं न कहूं, तो पूरा अठवाड़ा निकल जाता है, और उन्हें ध्यान भी नहीं आता कि कपड़े मैले हो गए हैं। उनके दूध का, फलों का, कमरे की सफाई का मुझे ही प्रबंध करना पड़ता है। सोचती हूँ, यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरी बे-परवा मनमानी करने वाली स्त्री आ जाती तो क्या होता? घर में धूल उड़ने लगती। थोड़े ही दिनों में बीमार हो जाते। उन्हें अपने दफ्तर की सफाई का भी ध्यान नहीं। उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। नौकर सिर चढ़ा रखे थे, अब ये संभल गए हैं। ये निगोड़े आप-से-आप तो कोई काम करते ही नहीं। जब तक सिर पर न खड़े रहो, तब तक हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहते हैं। कभी-कभी मुझे उन पर भी क्रोध आ जाता है। वे क्यों दबदबे से काम नहीं लेते? मैं चार दिन के लिए बाहर चली जाऊं, तो घर में कीड़े रेंगने लगें।
एक दिन मैंने कहा- “सारे भारतवर्ष में तुम्हारी कविता की धाक बंधी हुई है, परन्तु क्या यह भी किसी को पता है कि तुम इतने बेपरवा, ऐसे आलसी हो?”
उन्होंने हँसकर उत्तर दिया—“तुम एक लेख न लिख दो। ”
“बदनाम हो जाओगे।”
“उसमें कुछ भाग तुम्हें भी मिल जायेगा।”
“मैं क्यों लेने लगूं? तुम हँसकर टाल देते हो। तनिक सोचो तो सही, ऐसी बेपरवाही भी किस काम की?”
“मैंने तुम्हें घर की रानी बना दिया।”
मैंने धीरे से कहा—“घर की रानी तो मैं बनी, परन्तु तुम अपने दफ्तर की ओर तो ध्यान करो।”
“मैं तुम्हें अपना सुपरिन्टेन्डेन्ट समझता हूँ।”
मैं रूठकर चली गई। परन्तु हृदय आनंद के हिलोरे ले रहा था; जिस प्रकार चन्द्रमा का प्रतिबिंब जल पर तैरता है। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं उनके दफ्तर की और गई, तो दरवाजे के पास एक छोटा-सा बोर्ड लटकता देखा। उस पर लिखा था—
सावित्री देवी, बी.ए., सुपरिन्टेन्डेन्ट।
मैंने उसे जल्दी से उतारकर उनके सामने जा फेंका, और कहा—“ये शरारतें देख लोग क्या कहेंगे?”
उन्होंने मेरी ओर देखा तो मुस्कराकर भुजायें फैला दीं।
(6)
संध्या का समय था। मैंने अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनी, और पास जाकर कहा—“बाहर चलोगे? घूम आयें?”
वे इस समय कविता में मग्न थे। धीरे से बोले, “इस समय बात न करो। बड़ा विचित्र भाव सूझा है, उसको प्रकट करने के लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ। ”
मुझे विष-सा चढ़ गया। कैसे पुरुष हैं—सदा अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं। इतना भी नहीं होता, मेरी किसी समय तो मान लिया करें। पहले मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, परन्तु अब तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे इनका हृदय प्रेम से शून्य हो गया है। हाँ, कविता में हृदय निकाल कर रख देते हैं।
मेरी आँखों से आग बरसने लगी, मुँह से बोली—“सदा कविता ही सूझती रहती है, या किसी समय संसार का भी ध्यान आता है?”
“इस कविता से कवि-संसार में शोर मच जायेगा। ”
“तुम्हें मेरा भी ध्यान है, या नहीं?”
“यह अपने हृदय से पूछो। ”
“मैं अपने हृदय से नहीं, स्वयं तुमसे पूछती हूँ। तनिक आँखें उठा कर उत्तर दो न। ”
“यह कविता देखकर फड़क उठोगी। ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं लिखी। ”
मैंने हताश-सी होकर कहा—“मेरी बड़ी इच्छा थी, कि आज थोड़ा घूम आती, इस कविता ने काम बिगाड़ दिया। जी चाहता है, कागज़ छीनकर दावात तोड़ दूं।”
“दावात कागज़ की हानि साधारण बात है, परन्तु ये विचार फिर न मिलेंगे। आज अकेली चली जाओ।”
“मेरा मन नहीं मानता।”
उन्होंने हाथ से इशारा किया, और फिर झुक गये। मेरे हृदय में बर्छी सी लगी। उन्हें कविता का ध्यान है, मेरा नहीं। संसार में नाम चाहते हैं, परन्तु घर में प्रेम नहीं चाहते। वहाँ से चली, तो हृदय पर बोझ-सा प्रतीत हुआ। अकेली सैर को निकल गई। परन्तु चित्त उदास था, सैर में जी न लगा। हारकर एक पुल पर बैठ गई, और अपनी दशा पर रोने लगी। इन आँसुओं को देखकर पहले बाबूजी व्याकुल हो जाते थे। विवाह हुआ, तो मेरे सुख-दुःख का भार एक कवि को सौंपा गया। परन्तु अब इन आँसुओं को देखने वाला कोई न था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था, जैसे मेरी नाव नदी के धार में वेग से बही जाती है, और उस पर कोई मल्लाह नहीं। मैं अपनी बेबसी पर कुढ़ती थी। कभी-कभी आँख उठाकर देख भी लेती थी, कि कदाचित् आ रहे हों। प्रेम आशा नहीं छोड़ता।
मेरी आँखें जल की ओर थीं। सोचती थी, यदि कोई शक्ति मंत्र-बल से मुझे जल की तरंग बना दे, तो गंगा की तरंगों में खेलती फिरूं। एकाएक आँखें झपक गईं, निंद्रा देवी ने इच्छा पूरी कर दी। मैं गंगा में गिर गयी। बहुतेरे हाथ-पाँव मारे, पर निकल न सकी, प्रवाह में बहने लगी।
सुधि आई, तो मैं घर पर थी। वे सामने खड़े थे, कुर्सी पर एक डॉक्टर बैठा था।
उन्होंने कहा—“अच्छी बची, इनका धन्यवाद करो। ये मेरे मित्र डॉक्टर मणिराम हैं। आजकल काशी में इनके नाम की पूजा होती है। नदी में न कूद पड़ते तो, तुम्हारा बचना असंभव था। ”
मैं धीरे-धीरे उठकर बैठ गयी। साड़ी को सिर पर कर लिया, और डॉक्टर साहब की ओर देखा, मगर आँखें न मिल सकीं। मैंने ‘परमात्मा आपका भला करे’—कहा, और आँखें झुका लीं। परन्तु हृदय में हलचल मची हुई थी। चाहती थी, वे उठकर चले जायें। मेरा विचार था, इससे मेरा धीरज वापस आ जायेगा। परन्तु जब वे चले गये, तब जान पड़ा, मैं भूल पर थी। व्याकुलता बढ़ गयी। पानी की सैर को गई थी। आग खरीद लाई।
(7)
मणिराम
रात हुई, परन्तु मेरी आँखों में नींद न थी। उसे सावित्री की आँखों ने चुरा लिया था। उसमें कैसा आकर्षण था, कैसी बेबसी थी, जैसे कोई कैदी लोहे के जंगले के अंदर से स्वतंत्र सृष्टि को देखता है, और आह भरकर पृथ्वी पर बैठ जाता है। उसकी आँखें बार-बार मेरी और उठती थीं, परन्तु वह उन्हें उठने न देती थी, जिस प्रकार माँ अपने अबोध बालक को पराये खिलौने पकड़ते देखकर गोद में उठा लेती हैं। उस समय बालक किस प्रकार मचलता है, कैसा अधीर होता है, चाहता है, कि माँ छोड़ दे तो खिलौना लेकर भाग जाये। यही दशा सावित्री की थी। सत्यवान वहीं डटा रहा। यदि दो मिनट के लिए भी उठ जाता, तो जी भरकर देख लेता। कैसी सुंदर है, जैसे चंपा का फूल!
दूसरे दिन दुकान को जा रहा तो, उसे दरवाजे पर खड़ा पाया। उसने मेरी ओर प्यासे नयनों से देखा और मुस्करा दिया। इस मुस्कराहट में बिजली थी। मेरा धैर्य छूट गया। दुकान पर जी न लगा। सारे दिन सांझ की प्रतीक्षा करता रहा। पल-पल गिनते दिन समाप्त हुआ और मैं घर को वापस लौटा। पैर भूमि पर न पड़ते थे। इस समय मैं ऐसा प्रसन्न था, जैसे किसी को कुछ मिलने वाला हो। सत्यवान के मकान के पास पहुँचा, तो पैर आप-से-आप रुक गये, आँखें दरवाजे पर जम गईं। सहसा वह अंदर से निकली, और दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने मुँह से कुछ न कह, परन्तु आँखों ने हृदय के पर्दे खोल दिए। इन आँखों में कैसा प्रेम था, कैसा चाव और उसके साथ स्त्रियों की स्वाभाविक लज्जा। चटनी में खटाई के साथ शक्कर मिली हुई थी। मैं मतवाला-सा हो गया, और झूमता-झामता घर पहुँचा—जैसे किसी ने शत्रु का दुर्ग विजय कर लिया हो।
कई दिन बीत गये। नयनों का प्रेम-पाश दृढ़ होता गया। अब उसे देखकर जी न भरता था। ओस की बूंदों से किसी की प्यास कब बुझी है? तृष्णा अपने पैर आगे बढ़ा रही थी। अंतःकरण सावधान करता था, जैसे भय के समय कोई लाल झंडी दिखा दे। परन्तु कामदेव उस ड्राइवर के समान परवाह न करता था, जिसने शराब पी ली हो। यह शराब साधारण शराब न थी। यह वह शराब थी, जो धर्म-कर्म सब चूल्हे में झोंक देती है और मनुष्य को बलात् भय के मुँह में डाल देती है। यह काम-वासना की शराब थी।
एक दिन बहुत रात गए घर लौटा। चित्त दुखी हो रहा था, जैसे कोई भारी हानि हो गई हो। परन्तु सावित्री दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैं गद्गद्, प्रसन्न हो गया। घाटा पूरा हो गया। सारा क्रोध और दुःख दूर हो गया। सावित्री ने कहा—“आज आपको बड़ी देर हो गयी। ”
परन्तु आवाज थरथरा रही थी।
मेरा कलेजा धड़कने लगा। शरीर पसीना-पसीना हो गया। छात्रावस्था में हमने सैकड़ों मुर्दे चीरे थे। उस समय भी यह अवस्था न हुई थी। एक-एक अंग कांपने लगा। मैंने बड़ी कठिनता से अपने आपको संभाला, और उत्तर दिया—“जी हाँ, कुछ मरीज देखने चला गया था, आप दरवाजे पर खड़ी हैं, क्या किसी की प्रतीक्षा है?”
“हाँ, उनकी राह देख रही हूँ।“
“क्या आज कोई कवि-सम्मेलन है?”
“कवि-सम्मेलन तो नहीं। एक जलसे में गए हैं, वहाँ उन्हें अपनी नवीन कविता पढ़नी है।“
“तो बारह बजे के पहले न लौटेंगे।“
सावित्री ने तृषित नयनों से मेरी ओर देखा, और एक मधुर कटाक्ष से ठंडी साँस भरकर कहा—“घर में जी नहीं लगता।“
“अभी तो आठ ही बजे हैं।“
“जी चाहता है, कि घड़ी की सुइयाँ घुमा दूं।“
मेरे पैर न उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई विचित्र नाटक हो रहा हो। परंतु कोई देख न ले, इस विचार से पैर उठाने पड़े। हमें धर्म का विचार हो, या न हो, परंतु निंदा का विचार अवश्य होता है। सावित्री ने मेरी ओर ऐसी आँखों से देखा, मानो कह रही है—“क्या तुम अब भी नहीं समझे?”
मैं आगे बढ़ा, परंतु हृदय पीछे छूटा जाता था। वह मेरे वश में न था। घर आकर चित्त उदास हो गया। सावित्री की मूर्ति आँखों में फिरने लगी। उसकी मधुर वाणी कानों में गूंजने लगी। मैं उसे भूल जाना चाहता था। मुझे डर था, कि इस कूचे में पैर रखने से निंदा होगी। मुझ पर उंगलियाँ उठने लगेंगी। लोग मुझे भलामानस समझते हैं। यह करतूत मेरा सर्वनाश कर देगी। लोग चौंक उठेंगे। कहेंगे—“कैसा भलामानस प्रतीत होता था, परंतु पूरा गुरुघंटाल निकला!” प्रैक्टिस भी कम हो जायेगी। वह विवाहिता स्त्री है। उसकी ओर मेरा हाथ बढ़ाना बहुत ही अनुचित है। परंतु ये सब युक्तियाँ, सब विचार जल की तरंगे थीं। जितनी जल्दी उठती हैं, उससे जल्दी टूट जाती हैं। वायु का हल्का-सा थपेड़ा उनका चिह्न तक मिटा देता है। मनुष्य कितना दुर्बल, कितना बेबस है!
दूसरे दिन मैं सत्यवान के घर पहुँचा। परंतु पैर लड़खड़ा रहे थे—जैसे नया-नया चोर चोरी करने जा रहा हो। उस समय उसका हृदय किस प्रकार धड़कता है। कहीं कोई देख न ले! मुँह का रंग भेद न खोल दे। कभी-कभी भलमनसी का विचार भी आ जाता था। पैर आगे रखता था, परंतु पीछे हट जाता था। परंतु मैंने एक छलांग भरी और अंदर चला गया। इस समय मेरे होंठ सूख रहे थे।
सत्यवान ने मुझे देखा, तो कुर्सी से उछल पड़ा, और बड़े आदर से मिला। देर तक बातें होती रहीं। सावित्री भी पास बैठी थी। मेरी आँखें बराबर उसके मुख पर अटकी रहीं। पहले चोर था, अब डाकू बना। सावित्री की झिझक भी दूर हो गई। बात-बात पर हँसती थी। अब उसे मेरी ओर देखने में संकोच न था। लज्जा के स्थान पर चपलता आ गई थी। यहाँ से चला तो ऐसा प्रसन्न था, जैसे इन्द्र का सिंहासन मिल गया हो। तत्पश्चात रास्ता खुल गया। दिन में की बार सावित्री के दर्शन होने लगे। रात को दो-दो घंटे उसके पास बैठा रहता। मेरा और सावित्री का आँखों-आँखों ही में मन मिल गया। पर सत्यवान को कुछ पता न था। कल्पना-सागर से विचारों के मोती निकालने वाला कवि, बहुत दूर तक दृष्टि दौड़ाने वाला तत्वदर्शी विद्वान अपने सामने की घटना को नहीं समझता था। उसकी कविता दूसरों को जगाती थी, परंतु वह स्वयं सोया हुआ था; उस अनजान यात्री के समान जो नौका में बैठा दूर के हरे-हरे ऊँची-ऊँची पहाड़ियों को देख-देख कर झूमता है, परंतु नहीं जानता कि उसकी नाव भयानक चट्टान के निकट पहुँच रही है। सत्यवान विनाश की ओर बढ़ रहा था।
( 8)
सावित्री
कितना अंतर है। मणिराम की आँखें हृदय में आग लगा देती थीं। निकट आते, तो मैं इस प्रकार खिंची जाती, जैसे चुंबक लोहे की सुई को खींच लेता है। कैसे भोले-भाले लगते थे, जैसे मुख में जीभ ही न हो। परंतु मेरे पास आकार इस प्रकार चहचहाते हैं, जैसे बुलबुल फूल की टहनी पर चहचहाती है। उनके बिना अब जी नहीं लगता था। मकान काटने को दौड़ता था। चाहती थी, मेरे पास ही बैठे रहें। किसी ने मुँह से तो नहीं कहा, परंतु आँखों से पता चला कि मुहल्ले की स्त्रियाँ सब कुछ समझ गई हैं। मेरी ओर देखतीं तो मुस्कराने लगतीं। इतना ही नहीं, अब वह भी अपने विचारों से चौंक उठे। कवि थे, कुछ मूर्ख नहीं। बेपरवाह थे, अब हाथ मल-मलकर पछताने लगे। संसार जीतते थे, परंतु घर गंवा बैठे। सदैव उदासीन रहते थे। रात को सो नहीं सकते थे। बात करती तो काटने को दौड़ते। आँखों में लहू उतर आता था। न खाने की ओर ध्यान था, न पीने की ओर। कई-कई दिन स्नान न करते थे। अब मुझे न उनके कपड़े बदलवाने का शौक था, न उनके खाने-पीने का प्रबंध करती थी। कभी इन बातों में आनंद आता था, अब इतने से जी घबराता था। कुछ दिन पश्चात् प्रयाग के एक प्रसिद्ध मासिक-पत्र में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई, जिसका पहला पद था—
भयो क्यों अनचाहत को संग।
कविता क्या थी, अपनी अवस्था का चित्र था। मेरी आँखों से आग बरसने लगी। शेरनी की नाईं बिफरी हुई उनके सामने चली गई और बोली—“यह क्या कविता लिखने लगे हो अब?”
उन्होंने मेरी ओर ऐसी आँखों से देखा, जो पत्थर को भी मोम कर देतीं। शोक और निराशा का पूरा नमूना थीं। धीरे से बोले—“क्या है?”
“यह कविता पढ़कर लोग क्या कहेंगे?”
“कवि जो कुछ देखता है, लिख देता है। इसमें मेरा दोष क्या है?”
मैंने तनिक पीछे हटकर कहा-“तुमने क्या देखा है?”
“सावित्री, मेरा मुँह न खुलवाओ। अपने आँचल में मुँह डालकर देख लो, मुझसे कुछ छिपा नहीं।“
मैंने क्रोध में कहा-“गालियाँ क्यों देते हो?”
“गालियाँ इससे लाख गुना अच्छी होतीं।“
“तो तुम्हें मुझ पर संदेह है?”
“संदेह होता तो रोना काहे को था, अब तो विश्वास हो चुका। कान धोखा कहा सकते हैं, परंतु आँखें भूल नहीं करतीं। मुझे यह पता न था कि मेरा घर इस प्रकार चौपट हो जायेगा।“
मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। पर प्रकृति, जहाँ दुराचार को जाना होता है, वहाँ निर्लज्जता को पहले भेज देती है। ढिढाई से बोली—“तुम कविता लिखो, तुम्हें किसी से क्या?”
“घावों पर नमक छिड़कने आई हो?”
“मेरी ओर देखते ही न थे। उस समय बुद्धि कहाँ चली गई थी?”
“मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। नहीं तो आज हाथ न मलता।“
“परंतु लोग तुम्हारी वाह-वाह कर रहे हैं। जिस पत्र में देखो तुम्हारी ही चर्चा है, पढ़कर प्रसन्न हो जाते होंगे।“
यह सुनकर वे खड़े हो गए। नेत्रों में पागलों की-सी लाली चमक रही थी, चिल्लाकर बोले—“अपनी मौत को न बुलाओ, मैं इस समय पागल हो रहा हूँ।“
“तो क्या मार डालोगे? बहुत अच्छा, वह भी कर डालो। अपने जी की इच्छा पूरी कर लो।“
उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, जिस प्रकार सिंह अपने आखेट को मारने से पहले देखता है, और झपटकर अलमारी की ओर बढ़े। मेरा कलेजा धड़कने लगा। दौड़कर बाहर निकल गई। मेरा विचार था, वे मेरे पीछे दौड़ेंगे, इसलिए घर के बाहर मैदान में जा खड़ी हुई। परंतु साँस फूली हुई थी। मृत्यु को सामने देख चुकी थी। परंतु वे बाहर न आये। थोड़ी देर पीछे ‘दन’ का शब्द सुनाई दिया। मैं दौड़ती हुई अंदर चली गई। देखा—वे फर्श पर तड़प रहे थे। मृत्यु का दृश्य देखकर मैं डर गई। परंतु मुझे दुख नहीं हुआ। कहीं मुकदमे की लपेट में न आ जाऊं, यह चिंता अवश्य हुई।
दो मास बीत गए थे। मैं अपने आँगन में बैठी मणिराम के लिए नेकटाई बना रही थी। मैंने लोकाचार की परवाह न करके उनसे विवाह का निश्चय कर लिया था। लोग इस समाचार से चौंक उठे थे। परंतु मैं उनके मरने से प्रसन्न हो रही थी। समझती थी, जीवन का आनंद अब आयेगा। अचानक नौकर ने आकार डाक मेरे सामने रख दी। इसमें एक पैकेट भी था। मैंने पहले उसे खोला। यह मेरे मृतक पति की कविताओं का संग्रह था। मैंने एक-दो कवितायें पढ़ीं। हृदय में हलचल मैच गई। कैसे ऊँचे विचार थे, कैसे पवित्र भाव, संसार की मलिनता से रहित। इनमें छल न था, कपट न था। इनमें आध्यात्मिक सुख था, शांति थी। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। एकाएक तीसरे पृष्ठ पर दृष्टि गई। यह समर्पण का पृष्ठ था। मेरा लहू जम गया। पुस्तक मेरे नाम समर्पित की गई थी। एक-एक शब्द से प्रेम की लपट आ रही थी। परंतु इस प्रेम और मणिराम के प्रेम में कितना अंतर था। एक चंद्रमा की चाँदनी के समान शीतल था, दूसरा अग्नि के समान दग्ध करने वाला। एक समुद्र की नाईं गहन-गंभीर, दूसरा पहाड़ी नाले के समान वेगवान। एक सच्चाई था—परंतु निःशब्द, दूसरा झूठ था—पर बड़बोला। मेरी आँखों के सामने से पर्दा उठ गया। सतीत्व के उच्च शिखर से कहाँ गिरने को थी, यह मैंने आज अनुभव किया। उठते हुए पैर रुक गये। मैंने पुस्तक को आँखों से लगा लिया और रोने लगी।
इतने में मणिराम अंदर आये। मुख आने वाले आनंद की कल्पना से लाल हो रहा था। उनके हाथ में एक बहुमूल्य माला थी, जो उन्होंने मेरे लिए बंबई से मंगवाई थी। वह दिखाने आए थे। मुझे रोते देखकर ठिठक गए, और बोले—“क्यों रो रही हो?”
“मेरी आँखें खुल गई हैं।“
“यह अपनी माला देख लो। कल विवाह है।“
“अब विवाह न होगा।“
“सावित्री, पागल हो गई हो?”
“परमात्मा मुझे इसी प्रकार पागल बनाए रखे।“
मणिराम आगे बढ़े। परंतु मैं उठकर पीछे हट गई, और दरवाजे की ओर संकेत कर बोली—“उधर।“
उस रात मुझे ऐसी नींद आई, जैसी इससे पहले कभी न आई थी। मैंने पति को ठुकरा दिया था, परंतु उनके प्रेम को न ठुकरा सकी। मनुष्य मर जाता है, उसका प्रेम जीता रहता है।
ताई ~ विश्वंभर नाथ शर्मा ‘कौशिक’ की कहानी