Chapter 23 Gaban Novel By Munshi Premchand
Table of Contents
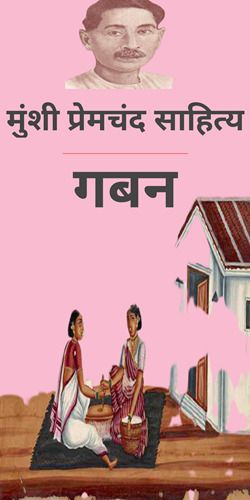
Chapter 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Prev | Next | All Chapters
एक महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है, जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है, और उसका पता लगा लेने वाले आदमी को पांच सौ रूपये इनाम देने का वचन दिया गया है, मगर अभी कहीं से कोई ख़बर नहीं आई। जालपा चिंता और दुःख से घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आख़िर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, ‘आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइये। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराये हुए आये, पर जालपा ने मायके जाने से इंकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, ‘क्या यहाँ पड़े-पड़े प्राण देने का विचार है?’
जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, ‘अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा, तो कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिये। अभागिनों के लिए वहाँ भी जगह नहीं है।’
दीनदयाल, ‘आख़िर चलने में हर्ज़ ही क्या है। शहजादी और बासंती दोनों आई हुई हैं। उनके साथ हँस-बोलकर जी बहलता रहेगा।
जालपा – ‘यहाँ लाला और अम्माजी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है, तो रोऊंगी।’
दीनदयाल, ‘यह बात क्या हुई, सुनते हैं कुछ कर्ज़ हो गया था, कोई कहता है, सरकारी रकम खा गए थे।’
जालपा – ‘जिसने आपसे यह कहा, उसने सरासर झूठ कहा।’
दीनदयाल – ‘तो फिर क्यों चले गये?’
जालपा – ‘यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे बार-बार ख़ुद यही शंका होती है।’
दीनदयाल – ‘लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? ‘
जालपा – ‘लालाजी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे। उन्हें घूमने का शौक था। सोचा होगा, यों तो कोई जाने न देगा, चलो भाग चलें।’
दीनदयाल – ‘शायद ऐसा ही हो कुछ लोगों को इधर-उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ़ हो, मुझसे साफ-साफ कह दो। ख़र्च के लिए कुछ भेज दिया करूं?’
जालपा ने गर्व से कहा, ‘मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दादाजी! आपकी दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है।
दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने पर राज़ी न हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, ‘यहाँ दिन-भर पड़े-पड़े रोने से तो अच्छा है।’
जालपा – ‘क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगी। और फिर रोने से क्यों डरूं, जब हँसना था, तब हँसती थी, जब रोना है, तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक-एक चीज़ में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी।’
दीनदयाल समझ गए कि यह अभिमानिनी अपनी टेक न छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गये। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने पचास रूपये का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, ‘इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, ‘मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
दादाजी, हाँ, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव है, आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो।’
दीनदयाल की आँखों में आँसू भर आये, नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आये।
क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल-शून्य टुकड़े कभी-कभी आकाश में दौड़ते नज़र आ जाते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ-खंडों की किलोलें देखा करती। चिंता-व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है? बादल के टुकड़े भांति-भांति के रंग बदलते, भांति-भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी रुठकर अलग-अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ-क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आख़िर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज़ रूपये लाते थे। कोई ख़ुशी से तो न दे देता।
यह रूपये देखकर वह कितनी ख़ुश होती थी। इन्हीं रूपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थीं। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल हैं। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें उसकी आँखों में अब कांटों की तरह गड़ती थीं, उसके ह्रदय में शूल की तरह चुभती थीं।
आख़िर एक दिन उसने इन चीज़ों को जमा किया, मखमली स्लीपर, रेशमी मोज़े, तरह-तरह की बेलें, गीते, पिन, कंघियाँ, आईने, कोई कहाँ तक गिनाये। अच्छा-खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबा देगी, और अब से एक नये जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे, आज उसकी यह गति हो रही है। आज वह इस मायाजाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें तो ऐसी सुंदर थीं कि उन्हें फ़ेंकते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीज़ों को उठा-उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो, हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आये, तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े-से-थोड़े में निर्वाह हो जाये। एक पैसा भी व्यर्थ न ख़र्च करेगी। अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से उसके नये जीवन का आरंभ होगा।
ज्योंही चार बजे, सड़क पर लोगों के आने-जाने की आहट मिलने लगी। जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा-स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर दस कदम भी चलना कठिन हो गया। बार-बार हाथ बदलती थी। यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर न पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे, पर वह इधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गये, तो उसने बेग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके।
वह घाट के समीप पहुँची, तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा, सिर झुकाकर मुँह छिपा ले, पर रतन ने दूर ही से पहचान लिया, मोटर रोककर बोली, ‘कहाँ जा रही हो बहन, यह पीठ पर बैग कैसा है?’
जालपा ने घूंघट हटा लिया और निद्यशंक होकर बोली, ‘गंगा-स्नान करने जा रही हूँ।’
रतन – ‘मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो, तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हें घर पहुँचाकर लौट जाऊंगी। बैग रख दो।’
जालपा – ‘नहीं-नहीं, यह भारी नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें देर होगी। मैं चली जाऊंगी।’
मगर रतन ने न माना, कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखती हुई बोली, ‘क्या भरा है तुमने इसमें, बहुत भारी है। खोलकर देखूं?’
जालपा – ‘इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज़ नहीं है।’
बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा, तो विस्मित होकर बोली, ‘इन चीज़ों को कहाँ लिये जाती हो?’
जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, ‘इन्हें गंगा में बहा दूंगी।’
रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, ‘गंगा में! कुछ पागल तो नहीं हो गई हो चलो, घर लौट चलो। बैग रखकर फिर आ जाना।’
जालपा ने दृढ़ता से कहा, ‘नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबाकर ही जाऊंगी।’
रतन – ‘आखिर क्यों?’
जालपा – ‘पहले कार को बढ़ाओ, फिर बताऊं।’
रतन – ‘नहीं, पहले बता दो।’
जालपा – ‘नहीं, यह न होगा। पहले कार को बढ़ाओ।’
रतन ने हारकर कार को बढ़ाया और बोली, ‘अच्छा अब तो बताओगी? ‘
जालपा ने उलाहने के भाव से कहा, ‘इतनी बात तो तुम्हें ख़ुद ही समझ लेनी चाहिए थी। मुझसे क्या पूछती हो, अब वे चीज़ें मेरे किस काम की हैं! इन्हें देख-देखकर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही न रहा, तो इन्हें रखकर क्या करूं? ‘
रतन ने एक लंबी साँस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, ‘बाबूजी के साथ तुम यह बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो, बहन, वे कितनी उमंग से इन्हें लाये होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक-एक चीज़ उनके प्रेम की एक-एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो।’ जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प-विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई, बोली, ‘यह बात नहीं है बहन! जब तक ये चीजें मेरी आँखों से दूर न हो जायेंगी, मेरा चित्त शांत न होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे ह्रदय पर अंकित है।’
रतन – ‘तुम्हारा ह्रदय बड़ा कठोर है। जालपा, मैं तो शायद ऐसा न कर सकती।’
जालपा – ‘लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ।’
एक क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोली, ‘उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, बहन! जो पुरूष अपनी स्त्री से कोई परदा रखता है, मैं समझती हूँ, वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती, तो यों तिलांजलि देकर न भागती। अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती, उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरूष में दुराव कैसा!’
रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ‘ऐसे पुरूष तो बहुत कम होंगे, जो स्त्री से अपना दिल खोलते हों। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो, तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई परदा न रक्खें। तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे परदा नहीं रखा?
जालपा ने सद्दचाते हुए कहा, ‘मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा।’
रतन ने ज़ोर देकर कहा, ‘झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ, अगर तुमने विश्वास किया होता, तो वे भी खुलते।’
जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा का तट आ पहुँचा। कार रूक गई। जालपा उतरी और बेग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, ‘नहीं, मैं इसे न ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गये।’
जालपा – ‘ऐसा कैसे समझ लूं।’
रतन – ‘मुझ पर दया करो, बहन के नाते।’
जालपा – ‘बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को ह्रदय में नहीं रख सकती।’
रतन ने भौंहें सिकोड़कर कहा, ‘किसी तरह न मानोगी?’
जालपा ने स्थिर भाव से कहा, ‘हाँ, किसी तरह नहीं।’
रतन ने विरक्त होकर मुँह उधर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेज़ी से घाट से उतरकर जल-तट तक पहुँच गई, फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ, उतना इन चीज़ों को पाकर भी न हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नानध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंत:करण में प्रकाश का ऐसा अनुभव न हुआ होगा। मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम-रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई, तो रतन ने पूछा, ‘डुबा दिया?’
जालपा – ‘हाँ।’
रतन – ‘बड़ी निष्ठुर हो’
जालपा – ‘यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती, तो आज यह दिन क्यों आता। कार चल पड़ी।
Prev | Next | All Chapters
Chapter 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
मुंशी प्रेमचंद के अन्य उन्पयास :
~ निर्मला मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास