Chapter 22 Gaban Novel ByMunshi Premchand
Table of Contents
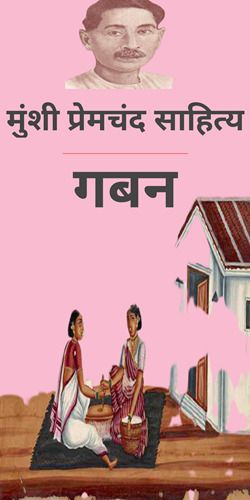
Chapter 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Prev | Next | All Chapters
एक सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई-कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह-तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ ग्यारह बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का खयाल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने ख़ुद आँखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्ज़ाम थोप रहे हैं। साफ-साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गये। इसने उसका नाकों दम कर दिया। पूछो, थोड़ी-सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज़ सैर-सपाटे और दावत-तवाज़े की क्यों सूझती थी। जालपा पर किसी को दया नहीं आती। कोई उसके आँसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सदबुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आँखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता!
एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे, तो मुँह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यों ही मुहर्रमी थी, उस पर मुँह लटका लेते थे, तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिज़ाज बिगड़ा हुआ है।
जागेश्वरी ने पूछा, ‘क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या?’
दयानाथ – ‘नहीं जी, इन तकषज़ों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ, उधर लोग नोचने दौड़ते हैं, न जाने कितना कर्ज़ ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी का देनदार नहीं हूँ। जाकर मेमसाहब से मांगो।
इसी वक्त ज़ालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गये। इन सात दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते-रोते आँखें सूज आई थीं। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी, बोली, ‘जी हाँ! आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें या तो समझा दूंगी, या उनके दाम चुका दूंगी।’
दयानाथ ने तीखे होकर कहा, ‘क्या दे दोगी तुम, हज़ारों का हिसाब है, सात सौ तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी कै पैसे दिए हैं तुमने?’
जालपा – ‘उसके गहने मौजूद हैं, केवल दो-चार बार पहने गए हैं। वह आए, तो मेरे पास भेज दीजिए। मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा, दस-पांच रूपये दीवान के ले लेगा।’
यह कहती हुई वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, ‘क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है, और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आँखों में आँसू भरकर बोली, ‘अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन!’
रतन – ‘यह बात क्या हुई, कुछ तुमसे तो कहा-सुनी नहीं हुई?’
जालपा – ‘ज़रा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे ज़िक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते, तो मैं रूपये दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आये और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ, कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रूपये जमा कर दिये।’
रतन – ‘मैं तो समझती हूँ, किसी से आँखें लड़ गई। दस-पाँच दिन में आप पता लग जायगा। यह बात सच न निकले, तो जो कहो दूं।’
जालपा ने हकबकाकर पूछा, ‘क्या तुमने कुछ सुना है?’
रतन – ‘नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है।’
जालपा – ‘नहीं रतन! मैं इस पर ज़रा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयाँ हों। मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।’
रतन ने हँसकर कहा, ‘इस कला में ये लोग निपुण होते हैं। तुम बेचारी क्या जानो!’
जालपा दृढ़ता से बोली, ‘अगर वह इस कला में निपुण होते हैं, तो हम भी ह्रदय को परखने में कम निपुण नहीं होतीं। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे, तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी।’
रतन – ‘अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो, तुम्हें कहीं घुमा लावें।’
जालपा – ‘नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घरवाले यों ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है?’
रतन – ‘कहीं नहीं, ज़रा बाज़ार तक जाना था।’
जालपा – ‘क्या लेना है?’
रतन – ‘जौहरियों की दुकान पर एक-दो चीज़ देखूंगी। बस, मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रूपये लौटा दिये। अब ख़ुद तलाश करूंगी।’
जालपा – ‘मेरे कंगन में ऐसे कौन-से रूप लगे हैं। बाज़ार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं।’
रतन – ‘मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ।’
जालपा – ‘उस नमूने का तो बना-बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र न आता हो, तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी।’
रतन ने उछलकर कहा, ‘वाह, तुम अपना कंगन दे दो, तो क्या कहना है! मूसलों ढोल बजाऊं! छः सौ का था न?’
जालपा – ‘हाँ, था तो छः सौ का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो ख़ुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे ख़ातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो, यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, ‘तुम जितना कहो, उतना देने को तैयार हूँ। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है। अभी मैं सब रूपये न दे सकूंगी, अगर दो सौ रूपये फिर दे दूं, तो कुछ हर्ज़ है?’
जालपा ने साहसपूर्वक कहा, ‘कोई हर्ज़ नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो।’
रतन – ‘नहीं, इस वक्त मेरे पास चार सौ रूपये हैं, मैं दिये जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे, तो किसी दूसरी जगह ख़र्च हो जायेंगे। मेरे हाथ में तो रूपये टिकते ही नहीं, करूं क्या जब तक ख़र्च न हो जायें, मुझे एक चिंता-सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो’
जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली, तो उसका दिल मसोस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना ख़ुश होता था।
आज वह होता, तो क्या यह चीज़ इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती! फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत ज़ब्त किया, पर आँसू निकल ही आये।
रतन उसके आँसू देखकर बोली, ‘इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है।’
जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, ‘क्यों, क्या मेरे आँसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ, नहीं यह मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी, तो मुझे तसल्ली रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना।’
रतन – ‘किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुःख इतना ही है, कि बाबूजी अब नहीं हैं। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आयेंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बडा दुःख हुआ। लोग कहते हैं, वकीलों का ह्रदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ, ज़रा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे।’
जालपा ने मुस्कराकर कहा, ‘बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा।’
रतन का विनोद-रंजित, प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा। मानो किसी ने उसे उस चिर-स्नेह की याद दिला दी हो, जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, ‘मुझे तो कभी यह ख़याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े हैं। मेरे ह्रदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग, यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन। क्या यह छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं?’
जालपा – ‘जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। दो घड़ी दिल बहलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल-डाल दौड़ता-फिरता है। समझ में नहीं आता, मुझसे इतना संकोच क्यों किया? यह भी मेरा ही दोष है। मुझमें ज़रूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी, जिसके कारण मुझसे परदा करना उन्हें ज़रूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुःख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है, उससे हम कोई भेद नहीं रखते।’
रतन उठकर चली, तो जालपा ने देखा, कंगन का बक्स मेज़ पर पड़ा हुआ है। बोली, ‘इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो।’
रतन – ‘ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है। अभी पूरे रूपये भी तो नहीं दिये!’
जालपा – ‘नहीं, नहीं, लेती जाओ। मैं न मानूंगी।’
मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिये खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से पाँच सौ रूपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ‘यह रूपये लीजिए, नारायणदास के पास भिजवा दीजिए। बाकी रूपये भी मैं जल्द ही दे दूंगी।‘
दयानाथ ने झेंपकर कहा, ‘रूपये कहाँ मिल गये?’
जालपा ने निसंकोच होकर कहा, ‘रतन के हाथ कंगन बेच दिया।’ दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे।
Prev | Next | All Chapters
Chapter 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
मुंशी प्रेमचंद के अन्य उन्पयास :
~ निर्मला मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास