Chapter 11 Gaban Novel By Munshi Premchand
Table of Contents
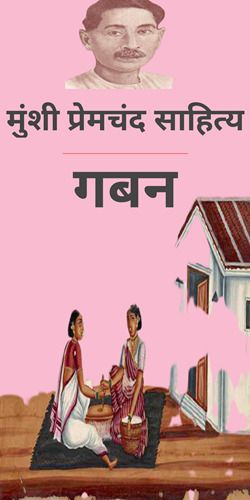
Chapter 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Prev | Next | All Chapters
दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी, उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते जाते थे। रमा को देखकर बोले – ‘आओ जी, रात क्यों नहीं आये? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते। सेठजी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बहार रही होगी!’
रमानाथ – ‘आपकी-सी सजावट तो न थी, हाँ और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्यायें भी आई थीं। मैं तो चला आया था; मगर सुना रातभर गाना होता रहा।’
रमेश – ‘सेठजी ने तो वचन दिया था कि वेश्यायें न आने पावेंगी, फिर यह क्या किया। इन मूर्खो के हाथों हिन्दू-धर्म का सर्वनाश हो जायेगा। एक तो वेश्याओं का नाम यों भी बुरा, उस पर ठाकुर-द्वारे में! छिः-छिः, न जाने इन गधों को कब अक्ल आवेगी।’
रमानाथ – ‘वेश्यायें न हों, तो झांकी देखने जाये ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं हैं।’
रमेश – ‘मेरा वश चले, तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत, हो तो आओ एक-आधा बाज़ी हो जाये।’
रमानाथ – ‘और आया किसलिए हूँ; मगर आज आपको मेरे साथ ज़रा सर्राफ़ तक चलना पड़ेगा। यों कई बड़ी-बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है; मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी।’
रमेश – ‘चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिलकुल कोरा हूँ। न कोई चीज बनवाई, न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है?’
रमानाथ – ‘लेना-देना क्या है, ज़रा भाव-ताव देखूंगा।’
रमेश – ‘मालूम होता है, घर में फटकार पड़ी है।’
रमानाथ – ‘जी, बिलकुल नहीं! वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ, तो मना करती हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गये, एक चीज़ भी नहीं बनी।’
रमेश – ‘मालूम होता है, कमाने का ढंग आ गया। क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रूपये जोड़ लिये?’
रमानाथ – ‘रूपये किसके पास हैं, वादे पर लूंगा।’
रमेश – ‘इस ख़ब्त में न पड़ो। जब तक रूपये हाथ में न हों, बाज़ार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुड्ढे नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं, उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यों मैं चाहूं, तो दो-चार हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भई, कर्ज़ की लत बुरी है।’
रमानाथ – ‘मैं दो-तीन महीनों में सब रूपये चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता, तो मैं ज़िक्र न करता।’
रमेश – ‘तो दो-तीन महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज़ से बड़ा पाप दूसरा नहीं। न इससे बडी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आये दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नज़र आओगे। बुरा न मानना। मैं जानता हूँ, तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज क़भी मत लो। गहनों का मर्ज़ न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया? जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रूपये केवल सोना-चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है, और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, उसमें उन्नति और उपकार की जो दो महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक-कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं, जहाँ होंठ छेदकर लोग गहने पहनते हैं।’
रमा ने कौतूहल से कहा – ‘याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक-कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मरज है, बहुत ही बुरा। वह धन, जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल-बच्चों का पेट काटकर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही। घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुँचे, न सही। मेवों और फलों के दर्शन उन्हें न हों, कोई परवाह नहीं, पर देवीजी गहने ज़रूर पहनेंगी और स्वामीजी गहने जरूर बनवायेंगे। दस-दस, बीस-बीस रूपये पाने वाले क्लर्को को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयस्सर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ, यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते।’
रमानाथ – ‘मैं तो समझता हूँ, ऐसा कोई भी देश नहीं, जहाँ स्त्रियाँ गहने न पहनती हों। क्या यूंरोप में गहनों का रिवाज नहीं है?’
रमेश – ‘तो तुम्हारा देश यूंरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं। वह धन लुटायें, उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फ़िज़ूल न खर्च होना चाहिए।’
रमेश बाबू इस वाद-विवाद में शतरंज भूल गये। छुट्टी का दिन था ही, दो-चार मिलने वाले और आ गये, रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी, जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रूपया न चुका सका, तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफ़ तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी तीन-चार महीने तक गहनों का नाम न लूंगा।
वह घर पहुँचा, तो नौ बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा – ‘आज सवेरे-सवेरे कहाँ चले गए थे?’
रमानाथ – ‘ज़रा बड़े बाबू से मिलने गया था।’
दयानाथ – ‘घंटे-आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते। गप-शप में दिन गंवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने-लिखने की उम्र है। इम्तहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा-सा खत लिखना पड़ जाता है, तो बगलें झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आये। मुझे नौकरी करते तीस साल हो गये। चाहता, तो अब तक हज़ारों रूपये जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुममें यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता।’
रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा – ‘किसने आपसे कहा है? ज़रा उसका नाम तो बताइये? मूंछें उखाड़ लूं उसकी!’
दयानाथ – ‘किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूंछें उखाड़ लोगे, इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ।’
रमानाथ – ‘बिल्कुल झूठ!’
दयानाथ – ‘बिल्कुल झूठ?’
रमानाथ – ‘जी हाँ, बिल्कुल झूठ?’
दयानाथ – ‘तुम दस्तूरी नहीं लेते?’
रमानाथ – ‘दस्तूरी रिश्वत नहीं है। सभी लेते हैं और खुल्लम-खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप-ही-आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता।’
दयानाथ – ‘सभी खुल्लम-खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती।’
रमानाथ – ‘दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं। मैं खुद न लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। आठ-आठ, नौ-नौ पाने वाले नौकर अगर न लें, तो उनका काम ही नहीं चल सकता मैं खुद न लूं, पर उन्हें नहीं रोक सकता।’
दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा – ‘मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है।’
यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गये। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निस्पृह बनकर क्या कर लिया, जो मुझे दोष दे रहे हैं। हमेशा पैसे-पैसे को मुहताज रहे। लड़कों को पढ़ा तक न सके। जूते-कपड़े तक न पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता, जब कि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता।
रमा घर में गया तो माता ने पूछा – ‘आज कहाँ चले गए बेटा, तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे।’
रमानाथ – ‘इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो। इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है।’
जागेश्वरी – ‘तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन-से झंडे गाड़ दिये! सारी ज़िन्दगी पेट पालते रहे।’
रमानाथ – ‘कहना तो चाहता था, पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी-कौड़ी को मुहताज रहे, वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती, तो भगत बन गये। यहाँ ऐसे घोंघा- बसंत नहीं हैं। बनियों से रूपये ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल्लगी नहीं है! जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया, बुद्धू है। लेने की तमीज़ नहीं, क्या करे बेचारा। किसी तरह आँसू तो पोंछे।’
जागेश्वरी – ‘बस-बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा, वह ज़रूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघारना आता है और किसी के सामने बात तो मुँह से निकलती नहीं। रूपये निकाल लेना तो मुश्किल है।’
रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया, तो जालपा ने उसे तीन लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिये। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिये, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियाँ पढ़ने लगा। चिट्ठियाँ क्या थीं, विपत्ति और वेदना का करूण विलाप था, जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था। केवल भावों का अंतर था, ‘ज़िन्दगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम, पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए, कभी-कभी हँस-बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ, न किसी को मुँह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रूपये जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं।’
रमा ने तीनों चिट्ठियाँ जेब में रख लीं। डाकखाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूं? कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता, तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर-भर जालपा के सामने रख देता, उसे किसी बड़े सर्राफ़ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो-जो चीजें लेनी हों, ले लो। कितनी अपार वेदना है, जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ, जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुँचाई थी। अगर वह जानता, उस अभिनय का यह फल होगा, तो कदाचित् अपनी डींगों का परदा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी, जब जालपा इस शोक-ताप से फुंकी जा रही थी, रमा को कर्ज़ लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका ह्रदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे ह्रदय से ईश्वर से याचना की,भगवन्, मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम-रोम से आत्मध्वनि-सी निकलने लगी – ईश्वर, ईश्वर! मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही। मुझसे क्यों परदा रखा और मुझसे परदा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया?
बरामदे में माल तौला जा रहा था। मेज़ पर रूपये-पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले, उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था, तो क्यों उसने विवाह करने से इंकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया।
जालपा ने उसे देखते ही पूछा, ‘मेरी चिट्ठियाँ छोड़ तो नहीं दीं? ‘
रमा ने बहाना किया, ‘अरे इनकी तो याद ही नहीं रही। जेब में पड़ी रह गई।’
जालपा – ‘यह बहुत अच्छा हुआ। लाओ, मुझे दे दो, अब न भेजूंगी।’
रमानाथ – ‘क्यों, कल भेज दूंगा।’
जालपा – ‘नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी,जो मुझे न लिखना चाहिए थीं। अगर तुमने छोड़ दी होती, तो मुझे दुःख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कराई।’
रमानाथ – ‘जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए।’
जालपा ने व्यग्र होकर पूछा – ‘तुमने चिट्ठियाँ पढ़ लीं क्या?’
रमा ने निद्यसंकोच भाव से कहा, ‘हाँ! यह कोई अक्षम्य अपराध है?’
जालपा कातर स्वर में बोली, ‘तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगे?’
आँसुओं के आवेग से जालपा की आवाज़ रूक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आँखों से आँसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगीं। एक क्षण में उसने स्वर को संभालकर कहा, ‘मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। जो चाहे सज़ा दो; पर मुझसे अप्रसन्न मत हो, ईश्वर जानते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुःख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई।’
जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुःख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें परदे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन ज़ाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं, हमसे ज़रा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है।
रमा जालपा के आँसू पोंछते हुए बोला – ‘मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ, प्रिये! अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है, क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता, तो अब तक मैंने किसी-न-किसी तरह दो-एक चीजें अवश्य ही बनवा दी होतीं। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है, जैसे मेहमान को पूछ-पूछकर भोजन दिया जाये। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी ‘नहीं-नहीं’ करता है। ईश्वर ने चाहा, तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतज़ार न करना पड़ेगा।’
जालपा ने सचिंत नज़रों से देखकर कहा, ‘तो क्या उधार लाओगे?’
रमानाथ – ‘हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज़ नहीं है। जब सूद नहीं देना है, तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता! हाथ में रूपया आ जाने से अलल्ले-तलल्ले खर्च हो जाते हैं। क़र्ज़ सिर पर सवार रहेगा, तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी।’
जालपा – ‘मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम न लूंगी।’
रमानाथ – ‘नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम क़र्ज़ से व्यर्थ इतना डरती हो। रूपये जमा होने के इंतज़ार में बैठा रहूंगा, तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते-देते साल में तीन-चार चीज़ें बन जायेंगी।’
जालपा – ‘मगर पहले कोई छोटी-सी चीज़ लाना।’
रमानाथ – ‘हाँ, ऐसा तो करूंगा ही।’
रमा बाज़ार चला, तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था, मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था।
Prev | Next | All Chapters
Chapter 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
मुंशी प्रेमचंद के अन्य उन्पयास :
~ निर्मला मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास