आवारागर्द आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी (Awaragard Acharya Chatursen Shastri Story) Awaragard Acharya Chatursen Shastri Ki Kahani एक आवारागर्द इंसान के प्रेम की कहानी है.
Awaragard Acharya Chatursen Shastri Story
Table of Contents
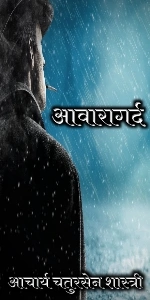
जो आवारागर्द नहीं, उन्हें आवारागर्दी के मजे कैसे समझाए जाएँ। लोग सभ्य हैं, इज्जत-आबरू वाले हैं, उनकी समाज में पद मर्यादा है, बहुत लोग उन्हें जानते हैं, वे यदि आवारागर्दी के चक्कर में पड़े, तो बस, सब खत्म। उनका रुआब उठ जाय, प्रतिष्ठा धूल मे मिल जाय, और देखनेवालों की नज़र से वे गिर जाय।
परन्तु मेरी बात ही निराली है। वह निरालापन आवारागर्दी में ही आ जाता है। बात यह है, न मेरी समाज में कोई इज्जत है न कोई मेरा भुलाकाती दोस्त है, न कहीं मेरा घरबार, ज़मीन-जायदाद है, न नौकरी, न लीडरी। न मैं कवि, न सपादक। मैं महज़ आवारागर्द हूँ जिधर मुँह उठा, चल दिया, जहाँ भूख लगी, खा लिया, जहाँ थक गया, सो गया, जो चीज़ चाही, माँगली, मौका मिला, चुराली, गरज जैसे वने, जीवन की गाड़ी चलाए जाना, दुःख शोक, चिंता और निराशा को पास न फटकने देना मेरी आवारागर्दी का खास रूप है, औरों की और जाने।
मन में जो सनक समाई, तो काश्मीर जा पहुँचा। कैसे? यह आप सभ्य पुरुष न समझ पाएंगे। फिर भी संक्षेप मे सुनिए रेल मे पूरा सफर किया बिना टिकिट। अक्सर टिकिट चेकर को चकमे दिए कभी पखाने में घुसकर और कभी दूसरी ओर आँख बचाकर, कूदकर। कभी पकड़े भी गए, तो हँस दिये, जेबे उलटकर दिखा दी। किसी ने गालियां देकर छोड़ दिया, किसी ने गर्दनिया देकर उतार दिया, किसी ने पुलिस के हवाले किया। मैं जानता हूँ, दुनियां में पद-पद पर विघ्न आते हैं, पर धुन के पक्के लोगों के सामने वे ठहर नहीं पाते। मेरे सामने भी ये विघ्न न ठहर सके। सिर्फ इतना हुआ, दो-चार दिन देर करके पीड़ी जा उतरा। आधी मंज़िल फतह हो गई। वहाँ से चला पैदल। रास्तेभर चट्टियों पर दूध, दही, पूरी और चाय-पानी का सामान बिक रहा था, पर अपने पास तो पैसा नहीं था। जब किसी भारी-भरकम को खाते देखता, सामने जाकर मुस्करा देता, और वह मुझे प्रायः खिलापिला देता। कभी गाकर, कभी हाथ देखकर पैसे बनाए। एक-दो बार बोझा भी ढोया, और सिर्फ एक बार चोरी की। आधा रास्ता पार हो गया।
एक दूकान पर बैठा गर्मागर्म पूरी-तरकारी उड़ा रहा था। सात पैसे जेब में थे, उनमे से छः पैसे की पूरी और सातवे का पान खा डालने का इरादा था। एक आदमी घबरा कर आया, और दूकानदार से पूछने लगा–“क्या पास मे कोई दवा-दारू की दूकान है? हमारे सेठ खड्ड मे गिर गए हैं, हड्डी-पसली चूरचूर हो गई है। पास मे कोई डाक्टर हो, तो फीस चाहे जो देनी पड़े, उसे बुलवा दीजिए।”
आदमी नवयुवक था। टूटी-फूटी हिंदी बोल रहा था। मैंने धीरे से दूकानदार से कहा “कहीं इस गधे से यह मत बता देना कि हम डॉक्टर हैं, नाहक हमें अटकना पड़ेगा। आए हैं तफरीह को, और बला सिर पड़ेगी। अरे भाई, नाक में दम है इन मरीज़ों के मारे, कमबख्त यहाँ भी दम नहीं लेने देते।”
दुकानदार ने क्षण-भर गौर से देखा, और यथा संभव आदर प्रदर्शन करके कहा–“डॉक्टर साहब, अब इस मुसीबत में तो इस बेचारे की मदद कर ही दीजिए।” फिर उसने जोर से युवक से कहा-“भाग्य की बात समझो कि डॉक्टर सामने बैठे हैं।”
युवक एकदम पास आकर मिन्नते करने लगा। मैंने कहा– “तो बुखार की तरह सिर पर क्यों चढ़े आते हो? बाबा, खा तो लेने दो, घबराओ मत; जाओ, कह दो-‘डॉक्टर साहब आते हैं।’ चुटकी बजाते सब ठीक हो जायगा।”
तसल्ली पाकर युवक दौड़ गया। मैं सोचने लगा अब डॉक्टरी धज बनाई जाय तो कैसे? मैला, फटा कोट, धूल-भरे पैर, दवा न दारू, और डॉक्टरी तो सात पीड़ी ने न की थी। कॉलेज मे जब पढ़ते थे, स्काउटिग मे नाम लिखा लिया था, पास में काम की चीज़ सिर्फ एक वेसलीन की शीशी थी, मैंने उसी से तमाम मतलब, हल करने की ठान ली,
जाकर देखा, कुछ चोट-ओट नहीं आई थी-न घाव हुआ न हड्डी टूटी, यों ही जरा खाल छिल गई थी, जितनी गंभीरता धारण की जा सकती थी, धारण करके मरीज देखा-कपड़ा माँगकर पट्टियाँ बनाई, और जरा-सी वेसलीन चुपड़कर लपेट दी, बाद में डॉक्टरी धज से साबुन से हाथ धोकर चल देने की ठानी, इतमीनान हुआ कि ५ रुपए अभी जेब में खनखना उठेंगे, श्रीनगर तक का चाय-पानी हो जायगा।
परतु सेठ कोई गुजराती गावदी था। हाथ जोड़कर बोला, “बैठ जाइए, डाक्टर साहब, अब आप जा नहीं पावेगे। आपको साथ चलना होगा। आपके आराम की पूरी व्यवस्था हो जायगी।
जै गंगा। थोड़ा नखरा करके मैं राजी हो गया। सवारी, कपड़े, चाय, टोस्ट, मक्खन, खाना, सब जुट गए। काशमीर में मजे की कटने लगी।
(2)
एक दिन सध्या-समय एक सकरी गली के सामने झूमता हुआ जा रहा था। क्यों? यह आप समझ जाइए। बदनाम मुहल्ला था, कभी-कभी उधर से यों ही घूम आया करता था। थोड़ी तबियत में गुदगुदी ही पैदा हो जाती थी। यहां और तो सब मौज-वहार थी, पर नकद नारायण जेव में न था, सेठ से कभी मांगा नहीं। और तिकड़म सब छोड़ दी थी। इसी से सिर्फ उधर घूमना मात्र ही हो जाता था, और कुछ नहीं।
हाँ, तो मैं एक सकरी गली के सामने झूमता हुआ जा रहा था। संध्या के धुंधले प्रकाश मे देखा–एक पुराने, छोटे-से मकान की दहलीज़ पर एक श्वेत-बसना स्त्री खड़ी एक वाबू से बाते कर रही है। अधेरे में ठीक-ठीक उसकी आयु और सुन्दरता नहीं भांपी जा सकी। परन्तु ज्यों ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, बाबू ने उस से कहा– “नमस्ते” और उसने भी हाथ जोड़ कर नमस्ते कहा। बाबू चल दिए। मगर उस स्त्री ने जो नमस्ते शब्द कहा, उसकी झंकार ने मेरे शरीर में रोमाच कर कर दिया, कुछ विचित्र मधुर स्वर था, फिर मैने सोचा इस बदनाम, गंदी गली मे ‘यह शुद्ध नमस्ते’ कैसा?
मैंने मुँह उठा कर देखा वह घर के भीतर लौट रही थी, मैंने साहस किया–एक कदम आगे बढ़कर कहा–“नमस्ते” वह लौटी, और आश्चर्य-चकित मेरी ओर उस अँधेरे में देखने लगी। मैने और निकट जाकर कहा-“आपने पहचाना नहीं-मैं डाक्टर हूँ।” मैंने ढेला फेका।
उसने भुनभुनाकर होंठों ही मे कहा-‘डाक्टर। फिर उसने सिर का पल्ला ठीक किया, हाथ जोड़कर उसी मधुर स्वर से नमस्ते किया, और उससे भी अधिक मीठे स्वर मे कहा-“आइए, भीतर आइए डाक्टर साहब!”
और, फिर हम एकदम मकान के भीतर। दरवाजे की कुंडी बंद कर दी गई। घर छोटा और साधारण था, पर साफ और सुरुचि-पूर्ण। कमरे में एक शतरजी विछी थी-कोने में पलँग था। दीवार से लगा एक लैंप टिमटिमा रहा था। शतरंजी पर बैठूँ या पलँग पर, यह निर्णय नहीं कर सका। उस पीली, धुंधली रोशनी मे मैंने फिर उसकी ओर देखा-एक दुबली-पतली, सुन्दर, छरहरी युवती थी। उम्र बीस से ऊपर होगी। बरबादी और वेदना की छाप उसकी आँखों और होठों पर थी।
उसने आगे बढ़कर, पलंग की ओर इशारा करके कहा” बैठिए।” सिर से टोपी उतारकर खूटी पर टाँग दी, बेत हाथ से लेकर एक कोने में रख दिया। फिर कहा “कोट उतारकर इतमीनान से बैठिए। इस वक्त कुछ गर्मी है, और आप बाहर से आए हैं। ठहरिए, खिड़की खोले देती हूँ। आप इतमीनान से बैठिए।”
मैं कोट उतारकर इतमीनान से बैठ गया। उसने खिड़कियाँ खोली, लैप जरा तेज़ किया, दो अगर-बत्तियाँ जलाईं, और चुपचाप पैरों के पास फर्श पर बैठ गई।
अभी दो मिनट भी न बीते थे कि ऐसा मालूम हुआ कि आवारागदी खत्म हो गई। मानो चिरकाल बाद शरीर और मन थकाकर अब घर लौटा हूँ, हालाँकि पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक मेरा कहीं घर था ही नहीं।
मेरा मुंह बद था। सोच रहा था, कौन है यह दुखिया, सुशीला स्त्री। इतनी मधुर, इतनी स्त्री-गुणों से विभूषित। परन्तु क्या उससे पूछूँ कि तुम कौन हो? इतनी आत्मीयता से परिपूर्ण स्वागत पाने पर भी। मैं चुप ही रहा। कभी उसे, कभी घर को घूर-घूरकर देखता रहा। उसने कहा-“चश्मा क्या हर वक्त लगाते हो! क्या रात मे बुरा नहीं मालूम होता?” उसने हाथ बढ़ाकर चश्मा आँखों से उतार लिया। गौर से आँखों को देखा-हथेली से आँखे दबाई। ओह! कितनी कोमल थीं वह हथेली।
मैंने दोनों हाथों से उसका हाथ थामकर कहा-“खूब मिलीं दोस्त।”
“तो क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे?”
“अजी तीन दिन से।” मैंने अटकल-पच्चू कहा।
“आपको यह मालूम कैसे हुआ कि मैं आ गई हूँ।”
मैंने शान से कहा-“वाह, यह भी कोई बात है,
आप यहाँ आवे, और मुझे न मालूम हो।”
वह गौर से देखने लगी। शायद यह भॉपने के लिये कि यह इतनी आत्मीयता से बाते करनेवाला है कौन, और मैं उसके मनोभाव समझकर मुस्कराने लगा।
एकाएक मैने कहा-“वहाँ फर्श पर क्यों बैठी हो, यहाँ बैठो।”
मैंने हाथ पकड़कर खींचा। उसने मेरे घुटनों पर सिर रखकर वेदना से टूटे स्वर मे कहा-“तुमने सुना तो होगा, साहब अब नहीं रहे। एक महीना हुआ, हार्ट फेल हो गया। मरने से दो-चार दिन पहले तो चिट्ठी आई थी-पढ़ो तो, देखो, क्या लिखा है।”
वह लपक कर उठी, एक पुलिदा बहुत-सी चिट्ठियों का रूमाल मे बंधा था, उठाकर खोला-एक खत निकालकर पढ़ा-“मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी” फिर कहा-“आप खुद पढ़िये”
मैंने आगे पढ़ना शुरू किया–“तुम राजी-खुशी काश्मीर..” उसने बाधा देकर पत्र को दोनों हाथों से ढांप लिया, और ऊपर की पंक्ति पर मेरी उंगली रखकर कहा–“यहां से पढ़िये”
मैंने पढ़ा–“मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी।” उसने मेरे साथ प्रत्येक अक्षर को दुहराया, उसकी आँखों से आँसुओं की धार वह चली, और वह फिर मेरे घुटनों पर सिर रख कर सिसकने लगी,
मैं घपले मे पड़ गया, सच कहूँ, मैं इतना द्रवीभूत होगया कि उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरने लगा, कुछ देर बाद मैंने कहा-“लाओ, चिट्ठी पढ़ूँ तो।” उसने चिट्ठी मोड़कर कहा-“मत पढ़ो मत पढ़ो-मैं सुन नहीं सकती, जिन्होंने लिखी थी, वह अब नहीं हैं, उन्होंने इतने खत लिखे हैं, गिनकर देखो, कितने हैं, पर अब नहीं लिखेगे, उसने ऊपर मुँह उठाया-टपाटप आँसू गिर रहे थे, होंठ काँप रहे थे, उसने घुटनों के बल उकसकर अपने को मेरी गोद मे डाल दिया,
उस सुखद अनुभूति का कैसे वर्णन करूँ, उसके केश-गुच्छ मे खोंसे हुए फूल की सुगंध से, उसके प्रेमी हृदय के हाहाकार से, उसके कोमल गात्र के आलिगन से जैसे मैं अपने ही मे मूर्छित हो गया। मैंने सोचा-क्या यह मुझे अपना कोई पूर्वपरिचित समझती है, या इसे होश-हवास ही नहीं, मैंने भी तो अपनी बातों से उसे खूब मुगालते में डाला, खत में मैंने उसका नाम पढ़ लिया था–रुक्मिणी।
मैंने आर्द्र स्वर से कहा–“रुक्मिणी, इतना र ज न करो, जो चला गया, उस पर सब करो, और जो मिल गया, उसके लिये ईश्वर को धन्यवाद दो।”
मैंने एक वासना से ललचाई दृष्टि उसके शोक-कातर मुख पर डाली। उसने ऑसू पोंछ डाले। चुपचाप चिट्ठियाँ इकठ्ठी करके गॉठ बाँधी, और फिर उठकर दूसरे कमरे में चली गई। क्षण भर बाद आकर फिर बोली “कुछ पियोगे?”
मैंने वास्तविक अर्थ न समझ कर कहा “नहीं, प्यास नही है।”
उसने क्षण-भर ठहर कर कहा “कुछ पीते हो या नहीं?”
मैं अब समझा, और कहा “नही कभी नहीं पीता।”
उसने और निकट आकर कहा “खर्च नहीं करना होगा, घर में है। लाऊँ-थोड़ी पियो।”
इतनी देर बाद मुझे स्मरण आया कि यहाँ जो मैं वेफिक्री से पलंग पर बैठा शाही ठाठ से बाते कर रहा हूँ, सो गाँठ में तो फूटा पैसा भी नहीं। अब यहाँ से बिना कुछ दिए जाना कितना जलील काम होगा। यह सोचते ही मैं एकदम उठ खड़ा हुआ, और कहा “अच्छा, अब चला, फिर कभी आऊँगा।”
उसने मृदुल स्वर मे कहा–“यही हाल उनका था। कभी नहीं पीते थे, पीने को कहती थी, तो उठ कर चल देते थे। अच्छा, मत पियो, मगर जाओ मत। नाराज़ मत हो।” और वह एकदम आगे बढ़ कर मेरे ऊपर गिर पड़ी, जैसे बहुत-सी फूल-मालाएँ किसी ने ऊपर फेक दी हों। और, मैंने आत्मविस्मृत होकर उसे कसकर छाती से लगा लिया। मैंने तन-मन से द्रवित होकर कहा “इतना दर्द, इतना दुःख, इतना प्रेम लिए तुम इस गदे घर मे बैठी हो सजनी।”, और फिर मैंने उसके अनगिनत चुम्बन ले डाले। शिथिल-गात होकर मैं पलॅग पर पड़ रहा। उसने धीरे से मेरे वाहु-पाश से पृथक् होकर कहा-“नाराज़ मत होना- तुम इजाजत दो, तो मैं जरा-सी पीलूँ। न पिऊँगी, तो तुम से बात भी न कर सकूँगी।
मैंने कहा–“पियो मैं नाराज नहीं हूँ।”
पीकर जब वह आई, तो मुस्करा रही थी, आवाज़ करारी थी, शरीर में फुर्ती थी। उसने कहा- “बीड़ियाँ तो हैं, क्या सिगरेट मॅंगाऊँ”?
“कैसे कहूँ कि मॅंगाओ।” मेरे पास तो पैसे न थे। मैंने कहा “मगर मैं तो पीता-खाता नहीं।”
“इसका मतलब यह कि एकदम सत हो गए हो।” उसने लड़के को आवाज देकर बुलाया। एक रुपया उसे देकर कहा “कैची की सिगरेट एक पैकेट, माचिस और पान ले आ।” मैं चपचाप देखता रहा।
धीरे-धीरे जैसे मैं जगत् को भूल गया, अपने को भूल गया। रात को भूल गया, दिन को भूल गया। अपने को मैंने चुपचाप पलंग पर डाल दिया–शिथिल-गात और मूर्छित मन।
उसने सिगरेट निकाल कर मेरे होंठों मे लगा दी, और फिर जला दी। धीरे से सिर ऊँचा करके एक छोटा-सा तकिया नीचे रख दिया। दो पान के बीड़े मुँह मे रख दिए। उसने फिर अगरबत्तियाँ कमरे मे जलाई। चारो तरफ देखा, मेरे आराम के लिये जो कुछ किया जा सकता है, वह उसने सब कर दिया या नहीं। फिर वह कमरे के बाहर गई। मैं समझ गया, वह पीने गई है, अपना दर्द दूर करने के लिये। क्षण-भर बाद वह आई, और मेरे पैरों को गोद मे लेकर बैठ गई। उसकी कोमल हथेलियों का सुखद स्पर्श प्राणों को हरा करने लगा। मैं चुप था–वह भी चुप थी-लैप धीरे-धीरे टिमटिमा रहा था। रात का सन्नाटा बढ़ रहा। ऐसा प्रतीत होता था, अन्धकार से व्याप्त इस भूमण्डल पर केवल वह छोटा-सा घर ही आलोक की रेखा वखेर रहा है। और, नक्षत्र-लोक में केवल दो प्राणी ही जीवित है, मैं और वह। और, हम दोनों अटूट सुख-सागर मे डूब गए है।
मैं तो पहले ही अपनी आवारागर्दी की बात कह चुका हूँ। कहने को एक ही बात रह गई थी, वह यह कि स्त्री से यथार्थ परिचय जीवन में नहीं हुआ था। और, अब मैं सोच भी न सकता था कि स्त्री क्या है, उसका मूल्य क्या हैं।
एकाएक मैं जैसे चौक उठा। मैंने कहा “अब जाऊँगा मैं।”
उसने जैसे भयभीत होकर नेत्रों मे कहा “कहाँ? क्यों?”
मैंने कहा “मैने अभी खाना भी नहीं खाया है, माहराज बाट तकता होगा।”
“आह! तब तुमने कहा क्यों नहीं। खाना मैं मगवाती हूँ।” और, लाख मना करने भी उसने खाना मॅगवाया। मेरे सामने थाल रखकर वह पखा ले बैठी। मैने “यह नहीं, तुम्हें खाना होगा मेरे साथ।”
उसने कहा “तो पियो फिर तुम भी।” उसके नेत्रो मे एक गहरी वेदना थी। मैंने सहमति दी, और जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। कौन उसे सोच सकता है। एक आवारागर्द के जीवन का दूसरा अध्याय-लोग जिसे सुहागरात कहते है। सचमुच वही।
और प्रातःकाल–जब आँखों मे शराब और नींद की खुमारी बढ़ रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, शरीर झूम रहा था। अभी अधेरा था, उसने मुझे चूमा, कोट मेरे कंधो पर डाला। दोनों हाथों मे हाथ लेकर हंसी, और फिर कहा “नमस्ते।”
इतना तो मुझे होश था कि मैं खाली, बिना कुछ दिए, जा रहा हूँ। मैं लाज से मरा जा रहा था, पर मैने कुछ कहा नहीं। दो कदम आगे बढ़ाए। वह हाथ मे हाथ दिए साथ थी। उसने कान में होंठ लगाकर कहा “कल जल्द आना।”
और, फिर उसने द्वार पर आकर एक बार नमस्ते किया। वह हँसी, उसका पीला और सूखा चेहरा, वेदना पूर्ण, गहन आँखें, उस हँसी की आभा से जैसे दिप गईं।।
मैं बोला नहीं, बोल सका नहीं, उसी भाँति लड़खड़ाता हुआ- ऊषा से अलोकित एकांत सड़क पर लुढ़कता चला-जैसे स्वप्न मे चल रहा होऊँ। ओह, कैसी अभूतपूर्व, सुखद रात रही वह।
(3)
दो मास ऐसे बीत गए, जैसे खेल हो गया हो। हाँ, मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। उस नारी के हृदय का मैंने संपूर्ण अध्ययन कर डाला। उसके प्रियतम के संपूर्ण खत पढ़ डाले। वह भी डॉक्टर था, मेरे जैसा अवारागर्द नहीं, प्रतिष्ठित सिविल सर्जन। उसके बीवी थी, बच्चे थे, उसने इस प्रेम लतिका को पत्नी की ही भाँति घर में रक्खा था। वह उसकी पत्नी के साथ खाती, सोती, रहती और पत्नी ही समझी जाती थी। उसने मुझसे एकएक दिन की बाते कहीं। अपने छः वर्ष के स्वप्न-सुख के मधुर संस्मरण कहती हुई वह हँसी, रोई और नाची, उन्माद में आवेशित होकर।
मैं दिन-भर अपने सेठ के यहां रहता–कहना चाहिए सोता, और सध्या होते ही झूमता हुआ वहाँ आता, जहाँ सुखद सेज़, गर्म खाना, उन्मादक मद्य, मृदुल नारी एक साथ ही उपस्थित थी-सब झझटों और खटपटों से रहित। एक यंत्र की भाँति मैं उस सुख-सागर में डूब जाता। खाता-पीता, सिगरेट पीता, और कहने न कहने योग्य क्या-क्या करता न करता।
दिन बीतते गये, और एक बोझ मेरे हृदय पर लदता गया। मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। अभागिनी, असहाय नारी मुझे कहाँ से खिलाती-पिलाती है? कुछ देना तो होगा ही। परंतु कहाँ से? मैं जानता था, मेरा साथी सेठ कहाँ रुपए-पैसे रखता है। मैं सेठानी के जेबरों के रखने की जगह भी जानता था। सब मेरा विश्वास करते थे। मेरी रात की गैरहाजरी भी सबको सह गई थी। कोई मेरे राज को जानता न था। अंत में मैंने संकल्प किया–किसी तरह यह सब रुपया चुराकर उसे दे आऊँ। संकल्प दृढ़ होता गया, और मैं अवसर की ताक में लगा। अंततः एक दिन मुझे सफलता मिली। सब जेबर और रुपया लेकर मैं उसी भाँति झूमता-झामता चिर-परिचित मार्ग पर संध्या के धूमिल प्रकाश में आगे बढ़ रहा था। वह सब मैंने एक तरफ छिपा दिया, उसे मालूम नहीं हुआ। मैंने भी सोचा– बस, यही अंतिम रात है। फिर अब और नहीं। उस दिन मैंने उसे जी भरकर प्यार किया, बहुत किया। अपना हृदय और आत्मा मैंने उसे दे दिया। पिछली रातों की भाँति यह रात भी बीत चली, और ऊषा के अलोक मे जब उसने हँसकर ‘नमस्ते’ कही, तब मैंने चुपचाप, नीरव भाव से चिर-विदा कहा।
मैंने लोटकर नही देखा, और चला। सेठ के डेरे की ओर नहीं, लंबी, बलखाती, पेचीली पहाड़ी सड़क पर, जो नीचे की दुनिया की ओर जा रही थी। उसी आवारागर्दी के आलम में, जिसमें नया आनंद और मस्ती का झरना झर रहा था। दिन बीता, और सध्या-समय एक चट्टी पर, बाहर पड़ी बेच पर, पड़ा, हुआ मैं बीती रातों को सोच रहा था। सब कुछ सपना-सा दीख रहा था। आँखे झरते ही वह आती, देखती, प्यार करती, सिगरेट पिलाती, माथा सहलाती, परंतु आँख खुलने पर सुदूर आकाश के टिमटिमाते तारे, टूटी बेंच और अपना एकाकी अवारागर्दी जीवन!
रास्ते में खाता, पीता, सोता, बैठता, अपनी चिर-अभ्यस्त आवारागर्दी से चला आ रहा था। एक दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। सेठजी साथ मे थे-उनके क्रोध का ठिकाना न था-बक रहे थे, और मुट्ठीयाँ बाँध रहे थे। मैं हंस रहा था। एक अंगूठी मेरी उँगली में थी। उसी से पकड़ा गया। उतारना भूल गया था। सोचा था, चलती बार उसे पहनाऊँगा। मैंने चोरी स्वीकार की, पर माल कहाँ है, नहीं बताया। मुझे पीटा गया, और भी यातनाएँ दी गई, परंतु उन यातनाओं में, मार मे कितना सुख था, कितना मज़ा था। वे यातनाएँ उस प्रिय नारी के सुखद स्पर्श, कोमल प्रमालिगन से कहीं अधिक अच्छी लग रही थीं। और, जब जेल की कोठरी मुझे मिली, तो उस एकांत में मैं था, और उस सजनी की जाग्रत् स्मृति। ओह, इसके बाद तो फिर हमारा न कभी विछोह हुआ, न मिलन। मैं प्रतिक्षण एक ही बात सोचा करता हूँ-काश्मीर की उन मनोरम घाटियों में वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, जीवन के अंत तक प्रतीक्षा करेगी।